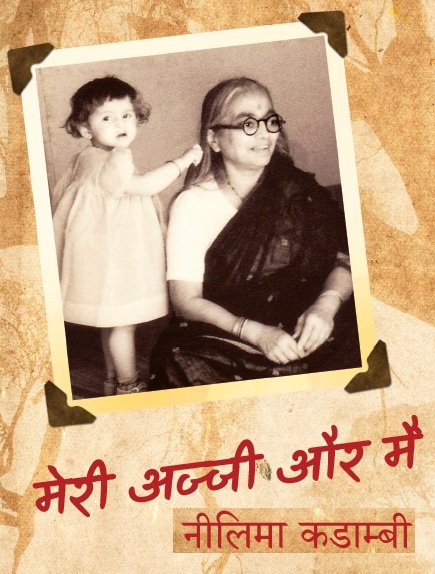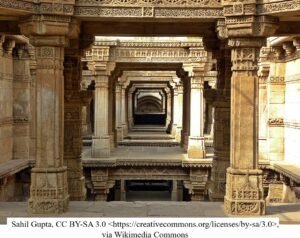विषय सूची (लिंक्स के साथ)
| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |
| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |
| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |
| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |
| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |
| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |
विवेक और मुझे एक बड़ा महत्वपूर्ण फ़ैसला करना था कि भारत लौटने के बाद हम कहाँ बसें । मेरे मन में यह बात हमेशा से थी कि रहेंगे हम भारत में ही । मुझे भ्रमण करने का, नए-नए स्थान देखने का, नए-नए लोगों से मिलने का और भिन्न-भिन्न संस्कृतियों को जानने-समझने का बड़ा शौक था, मगर किसी अन्य देश में बसने की इच्छा मुझे कभी नहीं हुई । यह बात मैंने विवेक को शादी के पहले ही बता दी थी और उन्होंने मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए ऐसा ही करने का वचन दिया था । विवेक के दो भाइयों ने अमेरिका जा बसने का फ़ैसला किया था और वहाँ रहते हुए उन्हें ग्रीन कार्ड भी मिल गए थे । जल्दी ही उन्हें वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी । मगर विवेक और मैंने रूस में उच्चतर अध्ययन और विशेषज्ञता का क्रम पूरा होने पर भारत लौटना ही तय किया ।
यहाँ बसने के लिए हमारे सामने तीन विकल्प थे– मुंबई, पुणे और बंगलौर । विवेक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करके भारत में कॉर्निया की शल्यक्रिया में अधुनातन लेज़र तकनीक लाना चाहते थे । इसके लिए उन्हें मुंबई सबसे अधिक उपयुक्त लगा । वहाँ लोगों की सोच आमतौर पर अधिक खुली होती है और वे इलाज़ पर ख़र्च में आनाकानी भी नहीं करते । मगर भारत की इस आर्थिक राजधानी में रहन-सहन काफ़ी महँगा था और जीवन की गुणवत्ता हलकी । पुणे मुंबई के नज़दीक ही था पर वहाँ की जलवायु बेहतर थी और वहाँ छोटे शहर की वे सुविधाएँ थीं जिनके हम दोनों ही अभ्यस्त थे । हमारे कॉलेज वाले बहुत से मित्र भी पुणे में ही बसे हुए थे इसलिए यहाँ व्यावसायिक संबंध सूत्र स्थापित करना भी ज़्यादा आसान था । विवेक के पिता ने सेवानिवृत्ति के बाद बंगलौर को ही अपना घर बना लिया था । माता-पिता दोनों की ही इच्छा थी कि उनके जिस एक बेटे ने भारत में रहना चुना है वह उनके साथ बंगलौर में ही रहे ।
बंगलौर का मौसम चूँकि बहुत सुहाना रहता था और यहाँ परिवार का साथ और सहारा भी था इसलिए यह आख़िरी प्रस्ताव हमें अधिक आकर्षक लगा । हमें न कन्नड़ आती थी न तमिल, मगर हमें पूरा विश्वास था कि ये भाषाएँ हम सीख ही लेंगे। आख़िर सोवियत संघ पहुँचने के तीन माह के अंदर हमने रूसी भाषा भी तो सीख ली थी ! इस फ़ैसले पर एक और महत्वपूर्ण प्रभाव इस बात का रहा कि श्रीसत्यसाईंबाबा का आश्रम तथा मानव सेवा के लिए बने अस्पताल बंगलौर के आसपास ही थे। ऐसे में उनके दर्शन के लिए हम प्रायः ही जा सकते थे और डॉक्टरों के रूप में उनके अस्पतालों में अपनी सेवाएँ अर्पित कर सकते थे जहाँ ग़रीबों की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है । अंततः इसी बात ने पलड़ा इस तरफ़ झुकाया कि हम इस ख़ूबसूरत शहर में अपने जीवन का नया दौर आरम्भ करें ।
हमें इस शहर में रहते बीस वर्ष से ऊपर हो गए हैं । विश्वास ही नहीं होता कि यह समय इतनी जल्दी कैसे गुज़र गया !
मैंने सर्जन बनने के लिए ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था और अब मैं सर्जन बन भी गई थी । सौभाग्य से मुझे बालशल्यचिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त करने का मौक़ा मिला । मुझे बच्चों के साथ काम करना हमेशा ही अच्छा लगता था ।
मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ चार-पाँच भिन्न-भिन्न अस्पतालों में बाहरी सलाहकार के रूप में काम करनेवाली दौड़-भाग भरी जिंदगी अपनाने के पक्ष में नहीं थी । इस समय मेरी नज़र में पूजा की देखभाल सबसे ज़रूरी काम था जिसके लिए मुझे समय की ज़रूरत थी । इसके लिए आसपास के किसी अस्पताल में काम करना ही मेरे लिए सबसे सुविधाजनक होता । मैं इंदिरानगर स्थित चिन्मय मिशन अस्पताल में गई । वहाँ के चिकित्सानिदेशक ने मुझे अगले दिन से ही सामान्य सर्जरी और बच्चों की सर्जरी, दोनों के ही लिए पूर्णकालिक शल्यचिकित्सक के रूप में कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव दिया । इस प्रस्ताव में बहुत ही सामान्य से वेतन के साथ ही डॉक्टरों के लिए अस्पताल के परिसर में ही बने दो-दो शयनकक्षोंवाले क्वार्टरों में एक क्वार्टर की सुविधा भी शामिल थी । मैं तो चिन्मय ट्रस्ट द्वारा संचालित मिशन अस्पतालमें काम करने के ख़याल से ही बहुत ख़ुश थी अतः यह प्रस्ताव मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया । विवेक सलाहकार के रूप में कुछ अस्पतालों में जाने के साथ ही अपनी निजी प्रैक्टिस के लिए भी चेम्बर जमाने में जुट गए – पर प्रैक्टिस के जमने में समय लगता है !
विवेक के माता-पिता का आग्रह था कि हम उन्हीं के साथ रहें ।
इंदिरानगर में उनका बड़ा सुंदर बँगला था – मेरे अस्पताल से कुल पंद्रह मिनट पैदल की दूरी पर । पूजा का स्कूल भी वहाँ से अधिक दूर नहीं था और साथ खेलने के लिए वहाँ आसपास उसी की उम्र के कई बच्चे भी थे । इंदिरानगर में साईंबाबा का मंदिर ‘साईं दर्शन’ नया-नया ही बना था और वहाँ नियमित भजनों के अतिरिक्त निःशुल्क चिकित्सा के कैंप और नारायण सेवा की गतिविधियाँ भी आरंभ हो गई थीं जिनमें हम हाथ बँटा सकते थे । मैंने यह व्यवस्था, कुछ हिचक के साथ ही, स्वीकार कर ली क्योंकि विवेक अपने माता-पिता के घर में अधिक खुश रहते। व्यक्तिगतरूप से मैं तो चिन्मय मिशन अस्पताल में डॉक्टरों के क्वार्टर में ही स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करती ।
यह समय हमारे जीवन में कुछ कठिन रहा । हमें अपना काम मेरी छोटी-सी तनख़्वाह से ही चलाना पड़ रहा था और आरंभ के कुछ वर्षों में हम सैर-सपाटों या छुट्टियों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। विवेक की प्रैक्टिस धीरे-धीरे जमने लगी थी । हमने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा और कोशिश भी की पर हर बार मेरा गर्भपात हो जाता था जिसका कोई डॉक्टरी कारण भी पता नहीं चल रहा था । दैहिक और भावनात्मक स्तर पर इसने मुझे बुरी तरह झकझोर दिया और कुछ समय मैं अवसाद (डिप्रेशन) से भी गुज़री । फिर मुझे पता चला कि रूस में समय बिताकर भारत लौटे कई दंपतियों को गर्भाधान में या फिर गर्भावस्था में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था । मैं अंततः इस निर्णय पर पहुँची कि वहाँ की निर्मम जलवायु, ताज़े फल-सब्ज़ियों की कमी और साथ ही मॉस्को के आसपास आणविक कचरे के जिन ढेरों की बात समाचारों में की जाती थी, उनके विकिरण के प्रभाव से ही मुझे गर्भधारण संबंधी उन समस्याओं का सामना करना पड़ा था । विवेक और मैंने फ़ैसला किया कि ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप जो स्वस्थ बिटिया हमें मिली है उसी के लिए हम उनके कृतज्ञ रहेंगे और उसके लिए किसी भाई-बहन को लाने का ख़याल हम छोड़ देंगे । अपने आप से मैंने कहा कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इकलौती संतान होने के कारण वह बिलकुल बिगड़ ही न जाए !
विवेक ने १९९४ में कडाम्बी लेज़र विज़न की स्थापना की । परम सौभाग्य था कि उन्होंने जो नया लेज़र उपकरण आयात किया था उसे स्वयं साईंबाबा का आशीर्वाद मिल पाया । दक्षिण भारत में पाँच वर्ष तक फ़ोटोरिफ़्रैक्टिव केराटेक्टोमी (Photorefractive Keratectomy –PRK) और लासिक शल्यक्रिया में केवल उन्हीं का एकाधिकार था । यह बिलकुल नवीनतम तकनीक थी जिसका आविष्कार मॉस्को केफ़्योदरोव नेत्र संस्थान में विवेक के वहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान ही हुआ था । इसलिए उन्हें आज भी इस क्षेत्र में अगुआ और विशेषज्ञ माना जाता है । तीन वर्ष तक वे संपूर्ण भारत के साथ ही एशिया और यूरोप में घूम-घूमकर भाषण और प्रशिक्षण देते रहे। आज के अनेक लासिक शल्यचिकित्सकों की सफलता और कौशल के पीछे विवेक के सुदक्ष प्रशिक्षण का हाथ है । उन्होंने तो अपने एक नेत्र चिकित्सक चाचा की विनिपेग में लेज़र नेत्र केंद्र खोलने में मदद करने के लिए तीन महीने अमेरिका और कैनाडा में भी बिताए । पूजा की देखभाल उसकी दादी माँ बड़े प्यार से कर लेती थीं इसलिए मैं भी प्रायः विवेक के साथ यात्रापर निकल जाती थी । हम दोनों ने ही इन अनुभवों का भरपूर आनंद लिया और बहुत अच्छा समय बिताया । विश्वस्तर पर इस तरह पहचान बन जाने और इस प्रकार अनुभव अर्जितकर लेने का विवेक के कैरियर और सर्जन के रूप में उनकी प्रतिष्ठापर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । वे हर सोमवार को अपराह्न में ह्वाइटफ़ील्ड स्थित साईंबाबा अस्पताल में आँखों का निःशुल्क ऑपरेशन करने लगे और आज तक कर रहे हैं ।
पूजा तेज़ी से बढ़ रही थी और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही थी । वह बहुत भाग्यशाली थी क्योंकि उसके दादा-दादी तो हर समय उसके साथ थे ही, पर उसकी परदादी और परनानी भी बीच-बीच में हमारे साथ रहने आया करती थीं । मेरी दादी सास उसकी पहली गणित शिक्षक थीं और वह इस विषय में अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी मैसूर पाटी (दादी) के आशीर्वाद और शिक्षण को देती है । पियानो बजाना सीखने में उसने संगीत के क्षेत्र में अपनी अनोखी प्रतिभा का परिचय दिया । उसे मधुर कंठस्वर का वरदान मिला था जिसका समुचित उपयोग इंदिरानगर की साईं समिति द्वारा संचालित बालविकास कक्षाओं में भजन गाने में हुआ करता था । पाँच से पंद्रह वर्ष की उम्र तक वह सप्ताहांत में लगनेवाली इन कक्षाओं में जाती रही । उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करनेवाले अधिकतर मामलों में मैंने उसके फ़ैसलों को मान्यता दी थी लेकिन इस बातपर मैं दृढ़ थी कि चाहे कुछ भी हो, शनिवार अपराह्न को होनेवाली बालविकास की इन कक्षाओं में वह अवश्य ही जाए । कभी-कभी उसे लगता भी था कि मैं बेकार ही ज़िदपर अड़ी हूँ, पर आज वह यह स्वीकार करती है कि इन कक्षाओं ने उसके जीवन पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डाला है । इन्हीं की बदौलत उसे साईं मंदिर में होनेवाली नृत्यनाटिकाओं में भाग लेने के अवसर मिलते थेऔर एक बार, जब वह लगभग आठ वर्ष की थी, उसे एक ऐसे प्रदर्शन के बाद स्वयं साईंबाबा का आशीर्वाद मिला । उसके बचपन का यह सचमुच बहुत ही विशेष अवसर था ।
चिन्मय मिशन अस्पताल में मैंने पूर्णकालिक कार्य छोड़कर अंशकालिक सलाहकारी आरंभ कर दी थी ताकि मैं विवेक की बढ़ती हुई प्रैक्टिस को व्यवस्थित करने में समय दे सकूँ । लासिक क्रियाविधि के लिए प्रक्रिया और नियमावली के निर्धारण में मैंने विवेक की सहायता की ताकि उसमें सामंजस्य और परिशुद्धता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही उसके दस्तावेज़ भी तैयार किए जा सकें । उपकरण मुहय्या करानेवाली अमेरिकी कम्पनी से हमें उपकरणों की सार-सँभाल और लेज़र के हेड बदलने आदि में कोई सहायता नहीं मिलती थी । लेज़र के हेड हर वर्ष बदलने होते हैं, इसलिए हमने ख़ुद यह काम सीखा । इसका प्रशिक्षण लेने के लिए विवेक कैनाडा गए और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के लिए हम दोनों यूरोप और अमेरिका के कुछ केंद्रों में गए । वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में ही स्वास्थ्य संबंधी सहायता और सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए मैंने इंदिरानगर होम हेल्थ सर्विस (IHS) भी शुरू की । इसकी प्रेरणा थी परदादी तथा परनानी की स्वास्थ्य संबंधी वे अनेक समस्याएँ जो हमारे साथ रहते समय उनके सामने आई थीं । हालाँकि हम दोनों ही डॉक्टर थे, मैंने देखा कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए काफ़ी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और परिवार के आगे कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं । मैंने जो यह सेवा शुरू की उसमें मुझे विवेक, अपनी सासू माँ जयंती और बेटी पूजा से बहुत सहारा और मदद मिली । हमने एक टीम के रूप में कार्य किया जिसमें हमारा तालमेल बहुत अच्छा था और हम परस्पर एक-दूसरों की ज़िंदगी और कैरियर के हिस्से बन गए ।
मुझ पर गठिया (रूमटॉइड आर्थराइटिस) का हमला हुआ । यह एक स्व-प्रतिरक्षित(ऑटोइम्यून) आनुवंशिक विकार था जिसका असर शरीर के छोटे-छोटे जोड़ों पर पड़ता है । ऐसी स्थिति में सर्जरी ठीक से कर पाना कठिन हो जाता है इसलिए मुझे अपने कैरियर में विकल्पों के बारे में सोचना पड़ा । इसके अतिरिक्त डॉक्टरी के पेशे में नैतिकता के गिरते स्तर को देखकर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और स्वास्थ्य सेवाओं की चढ़ती क़ीमतें भी मुझे परेशान कर रही थीं क्योंकि इस तरह ये सेवाएँ बहुतों की पहुँच के बाहर होती जा रही थीं । अतः चालीस की उम्र में मैंने अपने कैरियर में बड़े बदलाव का फ़ैसला किया । शल्यचिकित्सक के रूप में स्वास्थ्य सेवाएँ देने के स्थान पर मैंने देश में उस समय तेज़ी से बढ़ते स्वास्थ्य बीमा उद्योग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन का कार्य हाथ में लिया । मुझे लगा कि मैं यदि इन सेवाओं की गुणवत्ता और क़ीमत में कुछ सुधार कर सकी और चिकित्सक वर्ग के कार्य में अधिक पारदर्शिता और दायित्वबोध ला सकी तो यह स्वास्थ्यसेवाओं को मेरा कहीं बेहतर योगदान होगा ।