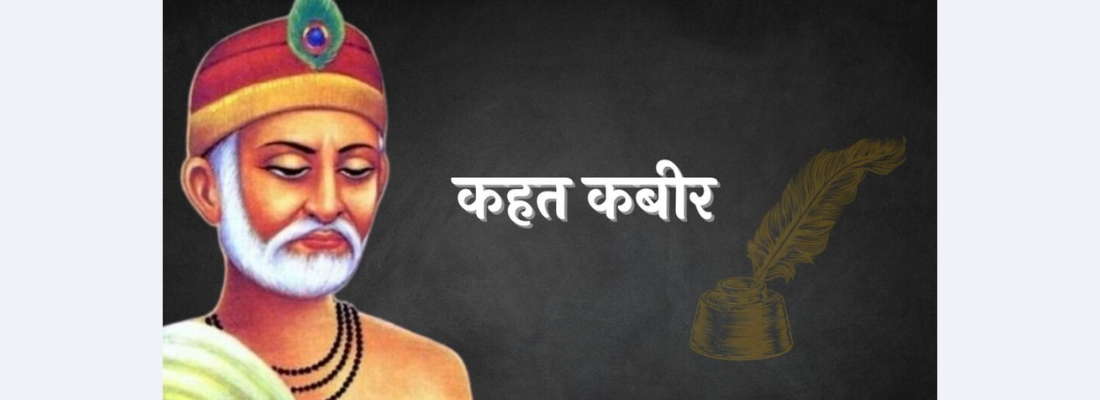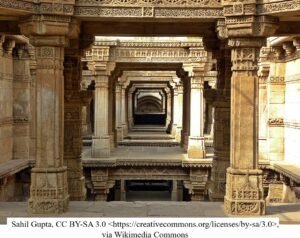बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर । // काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खानि ।
कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन — व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार; समाज की प्रचलित प्रथाओं, व्यवहारों और अंधविश्वासों; समाज में फैले ऊँच-नीच के भाव; जाति प्रथा की बुराइयों; सभी धर्म-संप्रदायों के व्यवहार में आए हुए अंधविश्वासों तथा पाखण्डों आदि — पर भी गहरा विचार किया है और अपनी रचनाओं में उन पर करारी टिप्पणियाँ भी की हैं। उनके मत में ये वे बुराइयाँ हैं जो समाज की सुख-शांति, सेहत और ख़ुशहाली के रास्ते में बाधा पैदा करती हैं कबीरदास जी के दोहों तथा अन्य रचनाओं को सही सही समझ पाने के लिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
— कुसुम बांठिया
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ।।
दुनिया में आमतौर पर उस व्यक्ति को बड़ा माना जाता है जिसके पास आम आदमी से अधिक ऊँचा और प्रतिष्ठावाला पद होता है; या जो अधिक शिक्षित और विद्वान होता है; या जो बहुत धनी और साधनसम्पन्न होता है । कबीरदास जी बड़प्पन के लिए इन विशेषताओं को कोई महत्व नहीं देते । ये विशेषताएँ समाज में व्यक्ति के कद को तो ऊँचा उठा देती हैं पर यदि वह व्यक्ति इन विशेषताओं से, या अन्य भी किसी प्रकार से समाज का कोई हित नहीं करता, समाज के लोगों की मदद या उनके सुख-सुविधा के लिए कोई काम नहीं करता, अपने साथ समाज को भी ऊँचा नहीं उठाता तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है । उसका बड़प्पन या ऊँचाई खजूर के पेड़ जैसी है । खजूर के पेड़ में पत्ते भी होते हैं और मीठे फल भी । मगर न तो उन पत्तों से धूप में चलते राहियों को छाया मिलती है, न उसके मीठे फलों तक कोई पहुँच पाता है । सच्चा बड़प्पन निःस्वार्थ भाव से लोगों के काम आने में होता है । अपने अन्य भी कई दोहों में कबीर ने परोपकार के गुण को बहुत महत्व दिया है ।

काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खानि ।
कहा मूर्ख कहा पंडिता, दोनों एक समानि ।।
कबीरदास जी मनुष्य की श्रेष्ठता की कसौटी उसकी बाहरी सांसारिक विशेषताओं को नहीं, बल्कि उसके आंतरिक गुणों को मानते थे । संसार में लोग अनपढ़ व्यक्ति को हीन और पढ़े लिखे पंडित को श्रेष्ठ मानते हैं । पंडितों, अर्थात विद्वान व्यक्तियों, को ही समाज अधिक सम्मान भी देता है । कबीर के मत में विद्या की यह कसौटी व्यर्थ है । जब तक मनुष्य में काम (इच्छाएँ, लालसाएँ), क्रोध (बदमिजाज़ी, कुढ़न, दुर्व्यवहार), मद (घमंड, औरों को नीचा समझने की भावना) और लोभ (लालच, अधिक से अधिक पाने की इच्छा और इसके लिए ग़लत काम करने से भी न हिचकना) आदि बुराइयाँ बनी और बसी रहती हैं, तब तक वह श्रेष्ठ माना ही नहीं जा सकता, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो । तब उसमें और अनपढ़ या मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर किया ही नहीं जा सकता ।
इस दोहे के माध्यम से कबीर लोगों को अपने आंतरिक दुर्गुणों से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं । साथ ही वे समाज को भी समझा रहे हैं कि उसे मनुष्य की श्रेष्ठता किस पैमाने (standard) से नापनी चाहिए ।
घट का शब्दार्थ ‘घड़ा’ या ‘मटका’ होता है । कबीर आदि संत कवियों ने इसका प्रयोग मानव शरीर के अर्थ में भी किया है जिसमें आत्मा निवास करती है । प्रायः इस शब्द के अर्थ में केवल देह नहीं, मन भी शामिल होता है ।
खानि का शब्दार्थ ‘खान’ (mine) होता है और इसका एक आशय ‘भंडार’ (storehouse) भी होता है । इस दोहे में मनुष्य के मन को वह खान या भंडार माना गया है जिसमें दुर्गुण पैदा भी होते रहते हैं और संचित भी रहते हैं ।

-
कहत कबीर ०३
ऊँचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय । // बुरा जो देखन मैं चला , बुरा न मिलिया कोय । ऊँचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय//बुरा जो देखन मैं चला , बुरा न मिलिया कोय// कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन…
-
कहत कबीर ०४
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर । // काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खानि । कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन — व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार; समाज की प्रचलित प्रथाओं,…
-
कहत कबीर ०२
निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी, छवाय । // जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप । कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन — व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार; समाज की प्रचलित प्रथाओं, व्यवहारों और अंधविश्वासों;…