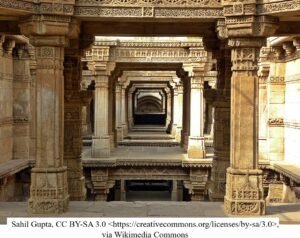बचपन में हम एक छोटी सी औद्योगिक बसाहट में रहते थे – तीन बँगले, ८-१० क्वार्टर, मजदूरों की बस्ती, एक डिस्पेंसरी और बैरकनुमा ऑफिसों के अहाते में एक राशन की दुकान – बस । अन्य सुविधाओं के लिए पास-दूर के गाँवों-कस्बों पर निर्भर रहना पड़ता था । ऐसी स्थिति में हमारे बड़े ही इंतज़ार, उत्साह और उल्लास का अवसर होता था नज़दीक के गाँव का तीन दिनी मेला । ठीक से याद नहीं, शायद दशहरे के समय ही लगता था यह ।
साल भर के उत्सुक इंतज़ार के बाद आने वाले इस मेले में हमें तीनों दिन तो नहीं, एक या दो दिन जाने का मौक़ा मिलता था । दिनों की संख्या इस बात से तय हो पाती थी कि दस-ग्यारह बच्चों के रेवड़ को सँभालकर सुरक्षित ले जाने-लाने के लिए कम से कम दो चुस्त और होशियार कारिंदों का इंतज़ाम हो पाता है या नहीं ।
मेले के ख़र्च के लिए हम भाई-बहन को एक एक दुअन्नी प्रतिदिन के हिसाब से मिलती थी । हालाँकि पैसे की क़ीमत उस समय आज की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, पर तब के हिसाब से भी साल में सिर्फ़ एक बार मिलने वाली यह रक़म कुछ कम ही थी । हमारे साथियों में कई को चवन्नी और बड़े बच्चों को तो अठन्नी तक मिल जाती थी । कुढ़ने से कोई लाभ भी नहीं था – “अपने बस में कुछ भी नहीं वो तो बाँटनेवाला बाँटे, कोई कारण होगा” (वैसे कारण भी हमें मालूम था । वे तत्कालीन मुद्रा की क़ीमत अपने बचपन की दरों से लगाते थे । बहरहाल . . . )।
जिस गाँव में मेला भरता था वह हमारे यहाँ से नज़दीक ही था । अपने गड़ेरियों की निगरानी में हमारी पदयात्रा शुरू होती । नन्ही सी मुट्ठी में अपनी निधि दबाए, नन्हे से दिल में आशाओं – आकांक्षाओं का उमड़ता सागर लिए हम उस कई बार देखी हुई चकाचौंध में फिर से भ्रमित हो जाते । प्रेमचंद की ‘ईदगाह’ के हामिद की तरह घूम-घूमकर सब कुछ देखते । गर्म रेत में भुनती मूँगफली का सोंधापन ललचाता । मुरमुरे के लड्डुओं पर भी नज़र जाती, पर अपनी पूँजी का आधा हिस्सा इन पर ख़र्च करने का हियाव न होता । एक तरफ़ वेश धारण किए कई जीवंत मानव मूरत बने सजे होते –रामचंद्र जी, महादेव, कार्तिक, काली माता . . . । दूसरी तरफ़ एक तंबू में जादू का खेला – प्रवेश टिकट दो आना । मुट्ठी और सख़्ती से भिंच जाती । क्या पता, खेला इतना ख़र्च करने लायक हो भी या नहीं ! सजी धजी चटकीली चमकती दुकानें ! खिलौने, पीपनी, लट्टू,चकरी ! कहीं देवी देवताओं की माटी की मूर्तियाँ या वुडकट । उस तरफ़ बाइस्कोप – ताजमहल से लेकर बारह मन की धोबन तक सब दिखलाने वाला – ढंग् – ढड़ंग् !!! बड़े बड़े चकडोल या झूलों पर दुअन्नी ख़र्च करने का कोई मतलब नहीं । कहीं उल्टी या चक्कर आ गए तो पैसे बरबाद ! अंदर का हामिद बहुत सोच समझकर जोखिम उठाने को तैयार होता था ।
पर होता क्या था ? चकरी ख़रीदने के बाद जाकर बिसाती की दूकान पर नीली चमचम चूड़ियाँ या पास की दूकान पर डोरी से फुदकता मेंढक नज़र आता था ! पर … सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया ! अगली बार के लिए और भी कंजूसी और सावधानी का संकल्प लिए लौटते । और कई बार तो इस सावधानी के चलते दुअन्नी जस की तस बचा भी लाते । कम से कम ग़लत चुनाव का पछतावा तो नहीं होता । वह तो बहुत बाद में जाकर समझ में आया – ग़लत या सही – कुछ न ख़रीदने का फ़ैसला भी तो एक चुनाव ही था । मन ही मन संकल्प करते, बड़े होकर इस तरह दुअन्नी के चक्कर में नहीं फँसना है ।
दशकों दशक गुज़र गए । दुअन्नी इतिहास बन गई । मेले – ठेलों के रंग रूप बदल गए । मुट्ठी में उदारता से खुलने की क्षमता आ गई । ललचाते हुए मन को मारने की ज़रूरत भी नहीं रही । पर … आज उम्र के बिलकुल विपरीत छोर पर सोचती हूँ, क्या यह दुअन्नी ज़िंदगी भर हमारे मन की मुट्ठी में बंद नहीं रही ? चाहे पंद्रह रुपए के आइसक्रीम की ख़रीद हो या सत्तर लाख के मकान की, पढ़ाई के विषय, जीवन पद्धति के चुनाव, शादी ब्याह, बाल बच्चे, सिनेमा थियेटर, सैर सपाटे, सेवा निवृत्त जीवन बिताने की व्यवस्थाएँ, देश के आम और ख़ास चुनाव – क्या हर समय दुनिया का मेला अपने अनगिनत विकल्पों की चकाचौंध से हमें भ्रमित नहीं करता रहा है ? और हम अपनी शारीरिक – मानसिक – आर्थिक क्षमताओं, अपनी परिस्थितियों, अपने कर्तव्यों आदि की दुअन्नी मुट्ठी में थामे, हर कदम पर चुनाव में उलझते नहीं रहे हैं ? चुनाव के बाद भी कभी ख़ुशी से आकाश पर उड़ते तो कभी ग़लत चुनाव पर उदासी के गड्ढे में गिरते नहीं रहे हैं ? क्या लोगों को कई बार ऐसा नहीं लगता कि बचपन में उस साल मेले में काग़ज़ की नाज़ुक चकरी ख़रीदने की जगह जादूगर के तंबू का टिकट ही ख़रीद लेना चाहिए था ? क्या पता ! वहाँ भूतों के नाच में ज़्यादा ही मज़ा आता !!!
— कुसुम बाँठिया
Image Credit: https://www.flickr.com/photos/ninara/49154301256