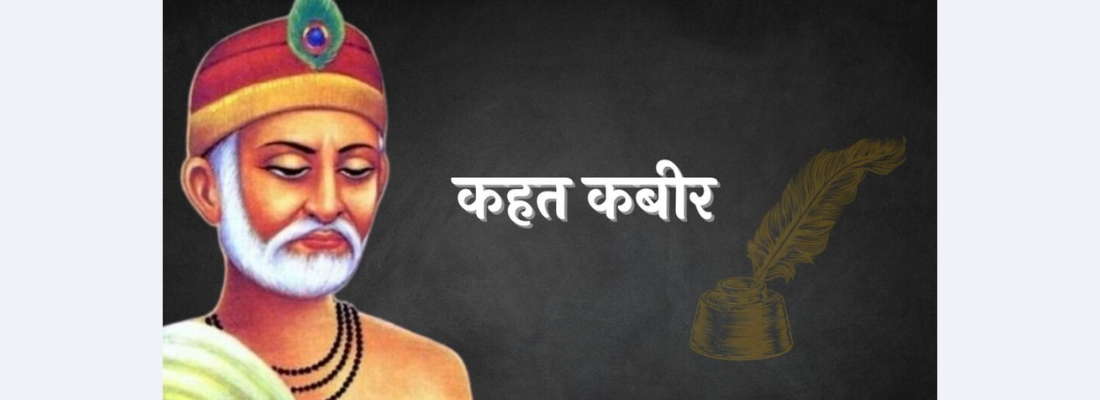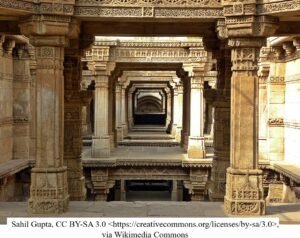ज्यों तिल माँहीं तेल है, चकमक माँहीं आगि । // ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय ।
कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन — व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार; समाज की प्रचलित प्रथाओं, व्यवहारों और अंधविश्वासों; समाज में फैले ऊँच-नीच के भाव; जाति प्रथा की बुराइयों; सभी धर्म-संप्रदायों के व्यवहार में आए हुए अंधविश्वासों तथा पाखण्डों आदि — पर भी गहरा विचार किया है और अपनी रचनाओं में उन पर करारी टिप्पणियाँ भी की हैं। उनके मत में ये वे बुराइयाँ हैं जो समाज की सुख-शांति, सेहत और ख़ुशहाली के रास्ते में बाधा पैदा करती हैं कबीरदास जी के दोहों तथा अन्य रचनाओं को सही सही समझ पाने के लिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
— कुसुम बांठिया
ज्यों तिल माँहीं तेल है, चकमक माँहीं आगि ।
तेरा साईं तुज्झ में, जाग सके तो जागि ।।
अपने अन्य कई दोहों की भाँति कबीर इस दोहे में भी इस बात पर बल दिया है कि ईश्वर का निवास मनुष्य के अंतर में ही होता है । ठीक जैसे तिल के दाने के अंदर तेल व्याप्त है और चकमक पत्थर के अंदर अग्नि का वास है पर ये बाहर दिखाई नहीं देते उसी प्रकार अंतर में स्थित ईश्वर भी बाह्य जगत में दिखाई नहीं देता । मनुष्य की भूल है कि वह बाहरी साधनों – मंदिर, मस्जिद, तीर्थयात्रा, पूजा, नमाज़ आदि – के माध्यम से उसे ढूँढ़ता है । जिस प्रकार पेरने से तिल में का तेल और रगड़ने से चकमक के अंदर की अग्नि का पता चलता है, उसी प्रकार अपने अंतर में ही ध्यान केंद्रित करके साधना करने से उसे अपने अंदर ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान होता है । मनुष्य का अज्ञान नींद की तरह होता है जिसके कारण उसे यथार्थ का ज्ञान नहीं होता । कबीर उसे अज्ञान की इस नींद से जागकर ज्ञान के प्रकाश में आने को कहते हैं ताकि उसे अपने अंतर में स्थित ब्रह्म का बोध हो सके ।

ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय ।
औरन को सीतल करै, आपहु सीतल होय ।।
कबीरदास जी अपने नीति और लोक व्यवहार संबंधी दोहों में सदा ऐसे आचरण का उपदेश देते हैं जिससे समाज में सौमनस्य तथा सुख शांति का प्रसार हो । प्रेम और सहिष्णुता को वे इसके लिए सबसे ज़रूरी गुण मानते हैं । इस दोहे में उन्होंने ‘आपा’ शब्द का प्रयोग अहंकार (Ego) के अर्थ में किया है । जब तक मनुष्य में अपने कुछ होने का भाव रहता है तब तक वह दूसरों से अपनेपन के साथ घुलमिल नहीं पाता । यह भाव पारस्परिक मेल मिलाप की राह में अड़चन बन जाता है । इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें अपने अहं भाव को त्यागकर औरों के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए, उनसे मिठास से बात करनी चाहिए । हम अगर औरों से मीठा बोलेंगे तो वे तो शीतल होंगे ही, अर्थात उन्हें तो सुख मिलेगा ही, स्वयं हमें भी बहुत अच्छा महसूस होगा । इसका कारण यही है कि हमारे मधुर व्यवहार से माहौल में जो मिठास, जो सौमनस्य आएगा, उसका सुख हमें भी महसूस होगा । कटु वचन और व्यवहार जहाँ कड़वाहट फैलाते हैं वहीं मीठे वचन और व्यवहार वातावरण को सुखद बनाते हैं । इससे समाज में भी सुख शांति बनी रहती है ।चन और व्यवहार वातावरण को सुखद बनाते हैं । इससे समाज में भी सुख शांति बनी रहती है ।

-
कहत कबीर ०३
ऊँचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय । // बुरा जो देखन मैं चला , बुरा न मिलिया कोय । ऊँचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय//बुरा जो देखन मैं चला , बुरा न मिलिया कोय// कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन…
-
कहत कबीर ०४
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर । // काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खानि । कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन — व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार; समाज की प्रचलित प्रथाओं,…
-
कहत कबीर ०२
निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी, छवाय । // जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप । कबीरदास जी संत कहे जाते हैं, पर इनके विचारों और रचनाओं का क्षेत्र केवल धर्म, अध्यात्म, चिंतन और भजन नहीं है। उन्होंने सांसारिक जीवन — व्यक्ति के चरित्र और व्यवहार; समाज की प्रचलित प्रथाओं, व्यवहारों और अंधविश्वासों;…